 भारत में सौर पैनल पर काम करता तकनीशियन
भारत में सौर पैनल पर काम करता तकनीशियन
भारत सहित दुनिया भर की कई अर्थव्यवस्थाएँ स्वच्छ विकास और हरित भविष्य के लिए प्रयास कर रही हैं । जैसे-जैसे अधिक से अधिक देश नवीकरणीय और टिकाऊ तरीकों की ओर बढ़ रहे हैं, तथाकथित "हरित नौकरियों" की मांग में तेज़ी से वृद्धि होने की उम्मीद है । लेकिन ये महत्वाकांक्षाएँ एक महत्वपूर्ण कारक पर टिकी हैं – कौशल । वर्तमान और भविष्य के दोनों श्रमिकों को हरित अर्थव्यवस्था में सफलता के लिए सुसज्जित करने की आवश्यकता होगी, और शिक्षा प्रणालियों को हर स्तर पर हरित कौशल विकास को एकीकृत करने की आवश्यकता होगी - प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से लेकर मध्य-करियर पुनः कौशलीकरण और उच्च कौशलीकरण तक । हरित परिवर्तन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षा प्रणालियां कितनी प्रभावी रूप से अनुकूलन कर पाती हैं, तथा तेजी से बदलती हरित अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आजीवन शिक्षा को अपना पाती हैं ।
हरित कौशल सिर्फ़ इंजीनियरों या वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं हैं - ये सभी क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ज़रूरी हैं । पानी की बचत और जलवायु-स्मार्ट कृषि तकनीकों को लागू करने वाले किसानों से लेकर अपशिष्ट को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को अनुकूलित करने वाले लॉजिस्टिक्स प्रबंधकों और इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण, संचालन और रखरखाव में लगे श्रमिकों तक, ये कौशल एक स्थिर भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं ।
हरित कार्यबल (वर्कफोर्स) चुनौती: स्थिर भविष्य के लिए कुशल कार्यबल का निर्माण
विश्व बैंक के शोध में पाया गया है कि भारत की केवल 5.9% नौकरियाँ ही हरित हैं, जबकि 4.6% कार्बन-गहन श्रेणी में आती हैं । इससे दोनों श्रेणियों से बाहर 89.5% नौकरियाँ रह जाती हैं, जो हरित अर्थव्यवस्था में बदलाव की चुनौती को रेखांकित करती हैं ।
अध्ययन में पाया गया है कि भारत में हरित और कार्बन-गहन नौकरियों का वितरण व्यापक रूप से भिन्न है । हरित नौकरियाँ अधिक आय वाले धनी राज्यों में केंद्रित हैं, जो तेजी से हरित परिवर्तन का संकेत देता है । (चित्र 1) ।

दोनों तरह की नौकरियाँ मुख्य रूप से पुरुष प्रधान हैं और युवा कर्मचारियों को आकर्षित करती हैं । फिर भी, नौकरी की गुणवत्ता में स्पष्ट असमानता है । जबकि हरित नौकरियाँ कार्बन-गहन नौकरियों की तुलना में बेहतर कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं, औसतन, वे नौकरी की सुरक्षा, लाभ और अनुबंध स्थिरता के मामले में अन्य नौकरियों से पीछे हैं । उल्लेखनीय रूप से, हरित नौकरियों में गैर-हरित नौकरियों की तुलना में 37% वेतन प्रीमियम होता है, जबकि कार्बन-गहन नौकरियों में 32% वेतन दंड होता है (चित्र 2) ।
श्रमिकों की हरित परिवर्तन में मदद करना
भारत को हरित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए, हरित रोजगार के अवसरों का विस्तार करना और श्रमिकों को आवश्यक हरित कौशल हासिल करने में सहायता करना आवश्यक होगा । इसे प्राप्त करने के लिए समन्वित नीतियों की आवश्यकता होगी जो श्रम बाजार सूचना प्रणालियों को मजबूत करें, कौशल विकास को बढ़ाएं और पारंपरिक उद्योगों से संक्रमण के लिए लक्षित समर्थन प्रदान करें ।
भारत पहले से ही इस चुनौती का सामना करने के लिए कदम उठा रहा है । 2015 में, इसने अपने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के हिस्से के रूप में हरित नौकरियों के लिए कौशल परिषद (SCGJ) की स्थापना की । यह उद्योग-नेतृत्व वाला संस्था अक्षय ऊर्जा, सतत विकास और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख हरित क्षेत्रों में बढ़ती मांग के साथ कौशल को संरेखित करने के लिए जिम्मेदार है । एससीजीजे द्वारा मानकीकरण और मान्यता पर जोर देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के वर्तमान और भविष्य के कार्यबल को राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के साथ-साथ दुनिया भर के हरित अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए ।
जून 2024 तक, एससीजीजे ने अक्षय ऊर्जा, अपशिष्ट और जल प्रबंधन, स्वच्छ खाना पकाने, पर्यावरण पर्यटन, वानिकी और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में 77 राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत योग्यताएँ विकसित की हैं । ये कौशल देश भर में 900 से अधिक संबद्ध शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि ई-लर्निंग सिस्टम कुछ प्रशिक्षणों को वर्चुअल रूप से संचालित करने में सक्षम बनाता है ।
इसका प्रभाव काफी अच्छा रहा है: अब तक 560,000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, तथा शिक्षक स्तर पर 4,717 प्रमाणित प्रशिक्षकों और 756 प्रमाणित मूल्यांकनकर्ताओं का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क विकसित किया गया है ।
भविष्य की गतिविधियां
विकसित, भारत को तीन प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी । सबसे पहले, भारत को समय के साथ हरित नौकरियों की प्रभावी निगरानी के लिए अपने श्रम बाजार सूचना प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता है । रुझानों पर नज़र रखने और कौशल अंतराल की पहचान करके, ये प्रणालियाँ शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश का मार्गदर्शन कर सकती हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उभरते हरित उद्योगों को आवश्यक कुशल कार्यबल तक पहुँच प्राप्त हो ।
दूसरा, औपचारिक शिक्षा और आजीवन सीखने की प्रणाली को मजबूत करना महत्वपूर्ण होगा । इससे भारत के वर्तमान और भविष्य के कार्यबल को सफल हरित परिवर्तन के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जा सकेगा और भारत के सतत विकास प्रयासों का समर्थन करने के लिए हरित-कुशल श्रमिकों की एक स्थिर श्रृंखला बनाने में मदद मिलेगी ।
अंत में, लोगों पर केंद्रित और समावेशी बदलाव के लिए एक स्पष्ट समझ की आवश्यकता होगी कि इस प्रक्रिया में किसे लाभ होगा और किसे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है । प्रभावित समूहों की पहचान करके और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए नीतियों को तैयार करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि हरित बदलाव के लाभ व्यापक रूप से साझा किए जाएं और कोई भी पीछे न छूटे । यह समावेशी दृष्टिकोण आर्थिक विकास और साझा समृद्धि दोनों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है क्योंकि भारत एक स्थिर भविष्य की ओर बढ़ रहा है ।


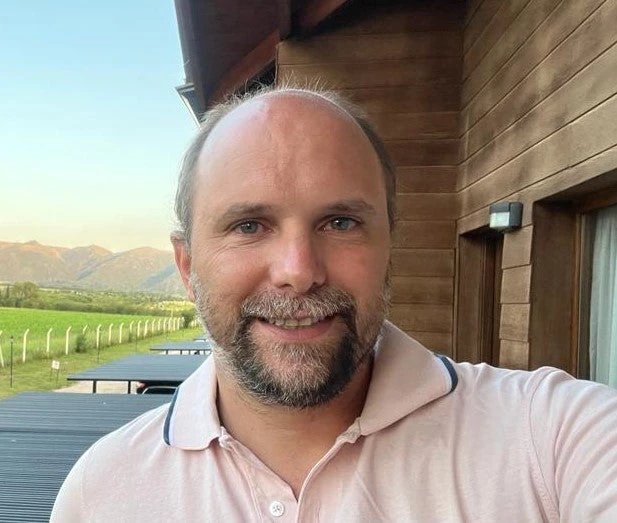

Join the Conversation